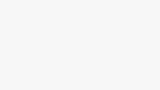गेटी इमेजेज़ के माध्यम से इंडिया टुडे ग्रुप
गेटी इमेजेज़ के माध्यम से इंडिया टुडे ग्रुपयह साल 1965 था.
रविवार को दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित एक छोटे से गांव जौंती में एक कठोर भारतीय किसान एक दौरे पर आए कृषि वैज्ञानिक के पास पहुंचा।
“डॉ साहबहम आपका बीज लेंगे,” उन्होंने कहा।
वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन थे, जिन्हें बाद में टाइम पत्रिका ने “हरित क्रांति के गॉडफादर” के रूप में प्रतिष्ठित किया और 20 वीं शताब्दी के भारत के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में गांधी और टैगोर के साथ स्थान दिया।
जब स्वामीनाथन ने पूछा कि किस बात ने किसान को उस दिन अपने प्रायोगिक उच्च-उपज वाले गेहूं को आज़माने के लिए प्रेरित किया, तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि जो कोई भी रविवार को अपने काम के लिए एक खेत से दूसरे खेत में घूमता रहता है, वह सिद्धांत से प्रेरित होता है, लाभ से नहीं, और यह उसका विश्वास अर्जित करने के लिए पर्याप्त था।
किसान का विश्वास भारत की किस्मत बदल देगा। जैसा कि प्रियंबदा जयकुमार की नई जीवनी, द मैन हू फेड इंडिया से पता चलता है, स्वामीनाथन का जीवन “नाव-टू-माउथ” अस्तित्व से खाद्य आत्मनिर्भरता तक एक राष्ट्र की छलांग की कहानी के रूप में पढ़ा जाता है, जो न केवल भारत के बल्कि खाद्य सुरक्षा के लिए एशिया के दृष्टिकोण को भी नया आकार देता है।
वर्षों की औपनिवेशिक नीतियों के कारण भारतीय कृषि स्थिर हो गई थी, पैदावार कम हो गई थी, मिट्टी ख़राब हो गई थी और लाखों किसान भूमिहीन हो गए थे या कर्ज़ में डूब गए थे। 1960 के दशक के मध्य तक, औसत भारतीय प्रतिदिन केवल 417 ग्राम भोजन पर जीवित रह रहा था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से अनियमित गेहूं आयात पर निर्भर था: अनाज जहाजों के लिए दैनिक प्रतीक्षा एक राष्ट्रीय आघात बन गई थी।
कमी इतनी गंभीर थी कि तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नागरिकों से गेहूं के स्थान पर शकरकंद का उपयोग करने का आग्रह किया, जबकि चावल, देश का मुख्य कार्बोहाइड्रेट, कम आपूर्ति में रहा।
“हरित क्रांति” ने सूखे खेतों को सुनहरी फसलों में बदल दिया, कुछ ही वर्षों में गेहूं की पैदावार दोगुनी कर दी और भुखमरी के कगार पर खड़े देश को एशिया के खाद्य महाशक्तियों में से एक में बदल दिया। यह अस्तित्व की सेवा में विज्ञान था, और स्वामीनाथन ने इसका नेतृत्व किया।
1925 में तमिलनाडु के कुंभकोणम में जन्मे स्वामीनाथन किसानों के एक परिवार में पले-बढ़े, जो शिक्षा और सेवा को महत्व देते थे। उनसे चिकित्सा का अध्ययन करने की अपेक्षा की गई थी, लेकिन 1943 के बंगाल के अकाल, जिसमें तीन मिलियन से अधिक लोग मारे गए, ने उन्हें जगा दिया।
उन्होंने अपने जीवनी लेखक को बताया, “मैंने ‘स्मार्ट’ फसलें उगाने के लिए एक वैज्ञानिक बनने का फैसला किया जो हमें अधिक भोजन दे सके… अगर दवा कुछ लोगों की जान बचा सकती है, तो कृषि लाखों लोगों की जान बचा सकती है।”
इसलिए उन्होंने प्लांट जेनेटिक्स की ओर रुख किया, कैम्ब्रिज में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और फिर नीदरलैंड और फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आईआरआरआई) में काम किया। मेक्सिको में उनकी मुलाकात अमेरिकी कृषि विज्ञानी और नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग से हुई, जिनकी उच्च उपज देने वाली बौनी गेहूं की किस्म “हरित क्रांति” की रीढ़ बन गई।
 गेटी इमेजेज के माध्यम से एएफपी
गेटी इमेजेज के माध्यम से एएफपी1963 में, स्वामीनाथन ने बोरलॉग को मैक्सिकन गेहूं की किस्में भारत भेजने के लिए राजी किया।
तीन साल बाद, एक राष्ट्रव्यापी प्रयोग के हिस्से के रूप में, भारत ने 18,000 टन इन बीजों का आयात किया। स्वामीनाथन ने भारतीय परिस्थितियों के तहत अनुकूलित और प्रजनन किया, जिससे सुनहरे रंग की किस्में पैदा हुईं जो बीमारी और कीटों का प्रतिरोध करते हुए स्थानीय गेहूं की तुलना में दो से तीन गुना अधिक उपज देती थीं।
जयकुमार लिखते हैं कि बीज आयात करना और जारी करना आसान नहीं था।
नौकरशाहों को विदेशी जर्मप्लाज्म पर निर्भरता का डर था, रसद ने शिपिंग और सीमा शुल्क को धीमा कर दिया, और किसान लंबी, परिचित किस्मों से चिपके रहे।
स्वामीनाथन ने डेटा और वकालत के साथ और अपने परिवार के साथ व्यक्तिगत रूप से खेतों में जाकर, किसानों को सीधे बीज देकर इन चुनौतियों पर काबू पाया। पंजाब में, उन्होंने रोपण के मौसम के दौरान त्वरित वितरण के लिए बीजों के पैकेट सिलने के लिए कैदियों को भी भर्ती किया।
जबकि मैक्सिकन छोटे अनाज वाला गेहूं लाल था, स्वामीनाथन ने यह सुनिश्चित किया कि संकर किस्में नान और रोटियों जैसी भारतीय ख़मीर वाली ब्रेड के अनुरूप सुनहरी हों। कल्याण सोना और सोनालिका कहा जाता है – “सोना” का हिंदी में अर्थ सोना है – इन उच्च उपज वाले अनाज ने पंजाब और हरियाणा के उत्तरी राज्यों को ब्रेडबास्केट में बदलने में मदद की।
स्वामीनाथन के प्रयोगों से भारत शीघ्र ही आत्मनिर्भर बन गया। 1971 तक, पैदावार दोगुनी हो गई, जिससे केवल चार वर्षों में अकाल अधिशेष में बदल गया, एक चमत्कार जिसने एक पीढ़ी को बचा लिया।
जयकुमार के अनुसार, स्वामीनाथन का मार्गदर्शक दर्शन “किसान पहले” था।
“क्या आप जानते हैं कि खेत भी एक प्रयोगशाला है? और किसान असली वैज्ञानिक हैं? वे मुझसे भी कहीं अधिक जानते हैं,” उन्होंने अपने जीवनी लेखक को बताया।
उन्होंने जोर देकर कहा कि वैज्ञानिकों को समाधान बताने से पहले सुनना चाहिए। उन्होंने सप्ताहांत गाँवों में बिताया और मिट्टी की नमी, बीज की कीमतों और कीटों के बारे में पूछा।
ओडिशा में, उन्होंने चावल की किस्मों को बेहतर बनाने के लिए आदिवासी महिलाओं के साथ काम किया। तमिलनाडु के शुष्क क्षेत्रों में उन्होंने नमक सहिष्णु फसलों को बढ़ावा दिया। और पंजाब में, उन्होंने संशयग्रस्त भूस्वामियों से कहा कि अकेले विज्ञान भूखमरी को ख़त्म नहीं करेगा और “विज्ञान को करुणा के साथ चलना चाहिए।”
स्वामीनाथन भारतीय कृषि के सामने आने वाली चुनौतियों से अच्छी तरह परिचित थे। राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने 2004 और 2006 के बीच पांच रिपोर्टों का निरीक्षण किया, जिसकी परिणति एक अंतिम रिपोर्ट में हुई, जिसमें किसानों के संकट और बढ़ती आत्महत्याओं की जड़ों की जांच की गई, जिसमें एक व्यापक राष्ट्रीय किसान नीति का आह्वान किया गया।
90 के दशक के अंत में भी वह किसानों के पक्ष में खड़े रहे; 98 साल की उम्र में, उन्होंने सार्वजनिक रूप से विवादास्पद भूमि सुधारों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा में विरोध करने वालों का समर्थन किया।
स्वामीनाथन का प्रभाव भारत से कहीं आगे तक फैला हुआ था।
जैसे 1980 के दशक में फिलीपींस में आईआरआरआई के पहले भारतीय महानिदेशक, उन्होंने पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में उच्च उपज वाले चावल का प्रसार किया, इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलीपींस में उत्पादन बढ़ाया।
मलेशिया से ईरान तक, मिस्र से तंजानिया तक, उन्होंने सरकारों को सलाह दी, कंबोडिया के चावल जीन बैंक के पुनर्निर्माण में मदद की, उत्तर कोरियाई किसानों को प्रशिक्षित किया, इथियोपिया के सूखे के दौरान अफ्रीकी कृषिविदों की मदद की, और एशिया भर में पीढ़ियों का मार्गदर्शन किया; उनके काम ने चीन के संकर चावल कार्यक्रम को भी आकार दिया और अफ्रीका की हरित क्रांति को बढ़ावा दिया।
 पल्लव बागला/कॉर्बिस गेटी इमेजेज़ के माध्यम से
पल्लव बागला/कॉर्बिस गेटी इमेजेज़ के माध्यम से1987 में, वह विश्व खाद्य पुरस्कार के पहले विजेता बने, जिन्हें भूख मिटाने में उनकी भूमिका के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा “जीवित किंवदंती” के रूप में सम्मानित किया गया।
चेन्नई में एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से उनका बाद का काम जैव विविधता, तटीय बहाली और जिसे उन्होंने “गरीब समर्थक, महिला समर्थक, प्रकृति समर्थक” विकास का मॉडल कहा, पर केंद्रित था।
हरित क्रांति की सफलता भी महत्वपूर्ण लागतों पर आई: गहन कृषि ने भूजल को ख़त्म कर दिया, मिट्टी ख़राब हो गई और कीटनाशकों से खेत दूषित हो गए, जबकि गेहूं और चावल की मोनोकल्चर ने जैव विविधता को नष्ट कर दिया और विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में जलवायु भेद्यता बढ़ गई।
स्वामीनाथन ने इन जोखिमों को पहचाना और 1990 के दशक में “सदाबहार क्रांति” का आह्वान किया: पारिस्थितिक क्षति के बिना उच्च उत्पादकता। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य की प्रगति उर्वरकों पर नहीं, बल्कि पानी, मिट्टी और बीजों के संरक्षण पर निर्भर करेगी।
एक दुर्लभ सार्वजनिक हस्ती, उन्होंने डेटा को सहानुभूति के साथ जोड़ा: उन्होंने अपने 1971 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का अधिकांश हिस्सा ग्रामीण छात्रवृत्तियों को दे दिया और बाद में “एग्रीटेक” के लोकप्रिय होने से बहुत पहले ही उन्होंने किसानों के लिए लैंगिक समानता और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया।
उनके प्रभाव पर विचार करते हुए, ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कहते हैं, “उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि भूख से मुक्ति सबसे बड़ी आजादी है।”
स्वामीनाथन के जीवन में, विज्ञान और करुणा ने मिलकर लाखों लोगों को यह आज़ादी दी। किसान-केंद्रित, टिकाऊ कृषि में एक स्थायी विरासत छोड़कर, 2023 में 98 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई।